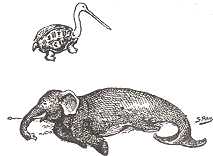अफलातून की ओर से सबको बड़े दिन का यह उपहार:
कद्दूपटाख
कद्दूपटाख
(अगर) कद्दूपटाख नाचे-
खबरदार कोई न आए अस्तबल के पाछे
दाएँ न देखे, बाएँ न देखे, न नीचे ऊपर झाँके;
टाँगें चारों रखे रहो मूली-झाड़ पे लटका-के!
(अगर) कद्दूपटाख रोए-
खबरदार! खबरदार! कोई न छत पे बैठे;
ओढ़ कंबल ओढ़ रजाई पल्टो मचान पे लेटे;
सुर बेहाग में गाओ केवल "राधे कृष्ण राधे!"
(अगर) कद्दूपटाख हँसे-
खड़े रहो एक टाँग पर रसोई के आसे-पासे;
फूटी आवाज फारसी बोलो हर साँस फिसफासे;
लेटे रहो घास पे रख तीन पहर उपवासे!
(अगर) कद्दूपटाख दौड़े-
हर कोई हड़बड़ा के खिड़की पे जा चढ़े;
घोल लाल रंग हुक्कापानी होंठ गाल पे मढ़े;
गल्ती से भी आस्मान न कतई कोई देखे!
(अगर) कद्दूपटाख बुलाए-
हर कोई मल काई बदन पे गमले पे चढ़ जाए;
तले साग को चाट के मरहम माथे पे मले जाए;
सख्त ईंट का गर्म झमझम नाक पे घिसे जाए!
मान बकवास इन बातों को जो नज़रअंदाज करे;
कद्दूपटाख जान जाए तो फिर हरजाना भरे;
तब देखना कौन सी बात कैसे फलती जाए;
फिर न कहना, बात मेरी अभी सुनी जाए।
इस कविता का अनुवाद सही हुआ नहीं था, इसलिए 'अगड़म बगड़म' में यह शामिल नहीं है। नानसेंस (बेतुकी) कविता संस्कृति सापेक्ष होती है और स्थानीय भाषा के प्रयोगों पर आधारित होती है। चूँकि हिन्दी क्षेत्रोंं में कई भाषाएँ प्रचलित हैं, ऐसा अनुवाद जो हर क्षेत्र में सही जम जाए, बहुत कठिन है। सुकुमार राय की मूल रचना में कई शब्द ऐसे हैं, जिनका न केवल सही अनुवाद ढूँढना मुश्किल है, उनसे मिलते जुलते शब्द भिन्न इलाकों में भिन्न हैं। पहले अनुच्छेद में 'मूली' दरअसल 'हट्टमूली' है, जिसे शायद जंगली मूली कहना ठीक होगा। इसी तरह 'लाल रंग' मूल रचना में 'आल्ता' है, जिसे प्रत्यक्षा या बिहार के लोग समझ जाएँगे, पर दूसरे इलाकों के लोग नहीं। बहरहाल, अगर सुनील को जँचे तो इसे कम से कम नेट पर तो डाला ही जा सकता है। इधर सुनील दस तारीख को बंगलौर आए थे, तब से उनका चिट्ठा लेखन बंद पड़ा है। जरा फिक्र हो रही है, सब ठीक तो है न!
मैं अपने नए मकान में आने के बाद से सुबह के ध्वनि प्रदूषण से दूर हूँ। लंबे समय के बाद पिछवाड़े में छोटा सा जंगल होने की वजह से सुबह चिड़ियों की आवाज सुन पाता हूँ।
कद्दूपटाख
कद्दूपटाख
(अगर) कद्दूपटाख नाचे-
खबरदार कोई न आए अस्तबल के पाछे
दाएँ न देखे, बाएँ न देखे, न नीचे ऊपर झाँके;
टाँगें चारों रखे रहो मूली-झाड़ पे लटका-के!
(अगर) कद्दूपटाख रोए-
खबरदार! खबरदार! कोई न छत पे बैठे;
ओढ़ कंबल ओढ़ रजाई पल्टो मचान पे लेटे;
सुर बेहाग में गाओ केवल "राधे कृष्ण राधे!"
(अगर) कद्दूपटाख हँसे-
खड़े रहो एक टाँग पर रसोई के आसे-पासे;
फूटी आवाज फारसी बोलो हर साँस फिसफासे;
लेटे रहो घास पे रख तीन पहर उपवासे!
(अगर) कद्दूपटाख दौड़े-
हर कोई हड़बड़ा के खिड़की पे जा चढ़े;
घोल लाल रंग हुक्कापानी होंठ गाल पे मढ़े;
गल्ती से भी आस्मान न कतई कोई देखे!
(अगर) कद्दूपटाख बुलाए-
हर कोई मल काई बदन पे गमले पे चढ़ जाए;
तले साग को चाट के मरहम माथे पे मले जाए;
सख्त ईंट का गर्म झमझम नाक पे घिसे जाए!
मान बकवास इन बातों को जो नज़रअंदाज करे;
कद्दूपटाख जान जाए तो फिर हरजाना भरे;
तब देखना कौन सी बात कैसे फलती जाए;
फिर न कहना, बात मेरी अभी सुनी जाए।
इस कविता का अनुवाद सही हुआ नहीं था, इसलिए 'अगड़म बगड़म' में यह शामिल नहीं है। नानसेंस (बेतुकी) कविता संस्कृति सापेक्ष होती है और स्थानीय भाषा के प्रयोगों पर आधारित होती है। चूँकि हिन्दी क्षेत्रोंं में कई भाषाएँ प्रचलित हैं, ऐसा अनुवाद जो हर क्षेत्र में सही जम जाए, बहुत कठिन है। सुकुमार राय की मूल रचना में कई शब्द ऐसे हैं, जिनका न केवल सही अनुवाद ढूँढना मुश्किल है, उनसे मिलते जुलते शब्द भिन्न इलाकों में भिन्न हैं। पहले अनुच्छेद में 'मूली' दरअसल 'हट्टमूली' है, जिसे शायद जंगली मूली कहना ठीक होगा। इसी तरह 'लाल रंग' मूल रचना में 'आल्ता' है, जिसे प्रत्यक्षा या बिहार के लोग समझ जाएँगे, पर दूसरे इलाकों के लोग नहीं। बहरहाल, अगर सुनील को जँचे तो इसे कम से कम नेट पर तो डाला ही जा सकता है। इधर सुनील दस तारीख को बंगलौर आए थे, तब से उनका चिट्ठा लेखन बंद पड़ा है। जरा फिक्र हो रही है, सब ठीक तो है न!
मैं अपने नए मकान में आने के बाद से सुबह के ध्वनि प्रदूषण से दूर हूँ। लंबे समय के बाद पिछवाड़े में छोटा सा जंगल होने की वजह से सुबह चिड़ियों की आवाज सुन पाता हूँ।